न्याय प्रणाली में मनुवादी सोच की पुनर्प्रतिष्ठा के प्रयासों को न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण का नाम दिया जा रहा है। नागरिक अधिकारों और संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय पर यदि ब्राह्मणवादी सोच हावी हो गई तब संविधान पर भी संकट आ सकता है।
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही संविधान के भारतीयकरण की मांग कट्टर हिंदूवादी संगठनों और भाजपा के कुछ बड़बोले बयानवीरों द्वारा उठाई जाती रही है। बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रखर विरोध के कारण सरकार संविधान से छेड़छाड़ का साहस तो नहीं कर पाई है किंतु संविधान का एक धर्म सम्मत पाठ तैयार करने की कोशिश अवश्य की गई है जो संविधान की मूल प्रवृत्ति से सर्वथा असंगत है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब संविधान को "हमारे लिए पवित्र 'गीता' महाग्रंथ के आधुनिक संस्करण की तरह" बताते हैं और राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद कहते हैं कि "हर सांसद का यह दायित्व बनता है कि वे संसद रूपी लोकतंत्र के इस मंदिर में उसी श्रद्धा भाव से अपना आचरण करें, जैसा कि वे अपने पूजा स्थलों में करते हैं" तब उनका संकेत संविधान के इसी धार्मिक पाठ की ओर होता है।
हम देखते हैं कि नए संसद भवन का "वैदिक रीति" से भूमि पूजन होता है और
इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश के प्राचीन गणराज्यों( जो वास्तव में कुलीन
तंत्र या ओलिगार्की द्वारा संचालित राज्य थे। इनकी सभाओं में गैर
क्षत्रियों, गुलामों और मजदूरों को स्थान नहीं दिया जाता था।) के हवाले से
यह दावा करते हैं कि हम दुनिया को यह कहने पर विवश कर देंगे कि इंडिया इज द
मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
पुनः संविधान दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि- हमारा संविधान
सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की
महान परंपरा, अखंड धारा उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है- संविधान की
प्रेरणाओं और मूल तत्वों के स्वदेशी उद्गम की ओर संकेत करता है।
वास्तविकता तो यह है कि संविधान के भारतीयकरण का विचार संविधान सभा के सम्मुख आया था और इसे खारिज करते हुए आंबेडकर ने कहा था- “मेरा विश्वास है कि यह ग्राम गणराज्य भारत के विनाश हेतु उत्तरदायी हैं। इसीलिए मैं प्रांतवाद और सांप्रदायिकता की निंदा करने वाले लोगों को ग्राम के प्रबल समर्थक के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हूँ। ग्राम आखिर है क्या, महज़ स्थानीयता की गंदी नाली, अज्ञानता, संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता का अड्डा ? मुझे प्रसन्नता है कि संविधान के प्रारूप में इस ग्राम का परित्याग कर व्यक्ति को इकाई के रूप में अपनाया गया है।”
आंबेडकर यह जानते थे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान में व्यक्ति को ही इकाई के रूप में स्वीकार करना होगा। इस बात के लिए जब उन पर औपनिवेशिक प्रभाव का आक्षेप भी लगाया गया तब भी वे विचलित नहीं हुए।
आंबेडकर ने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि आज की स्थिति में, जब हमारा सामाजिक मानस अलोकतांत्रिक है तथा राज्य की प्रणाली लोकतांत्रिक, ऐसे में कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा राजनीतिक दलों का भविष्य का व्यवहार कैसा होगा?
जब आंबेडकर यह इंगित करते हैं कि हमारा सामाजिक मानस अलोकतांत्रिक है तो
वे मनुवादी सोच की, सवर्ण वर्चस्व की, ब्राह्मणवादी शिकंजे की उस ऐतिहासिक
किंतु लज्जाजनक एवं अमानवीय परंपरा पर निशाना साधते हैं जो शोषण को चिर
स्थायी बनाने का जरिया थी।
आंबेडकर ने कहा- मुझे उन दिनों का स्मरण है, जब राजनीतिक रूप से जागरूक
भारतीय ‘भारत की जनता'- जैसी अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे।
उन्हें ‘भारतीय राष्ट्र' कहना अधिक पसंद था। हजारों जातियों में विभाजित
लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि इस शब्द के
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं,
हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता
को ठीक से समझ सकेंगे।
आंबेडकर यह जानते थे कि संविधान वंचित-शोषित और प्रताड़ित-अपमानित वर्ग का रक्षक तभी बन सकता है, तभी वह उन्हें सम्मानपूर्वक जीवनयापन का अवसर प्रदान कर सकता है जब वह देश की उस कथित गौरवशाली सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था की जकड़न से सर्वथा मुक्त हो जिसकी पुनर्प्रतिष्ठा की कोशिश आज संविधान के भारतीयकरण के माध्यम से हो रही है।
यह स्वाभाविक था कि मनुस्मृति पर गर्व करने वाली दक्षिणपंथी शक्तियों को इससे पीड़ा हुई। 30 नवंबर 1949 के ऑर्गनाइजर के संपादकीय में लिखा गया- "किन्तु हमारे संविधान में प्राचीन भारत में हुए अनूठे संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं हैं। मनु द्वारा विरचित नियमों का रचनाकाल स्पार्टा और पर्शिया में रचे गए संविधानों से कहीं पहले का है। आज भी मनुस्मृति में प्रतिपादित उसके नियम पूरे विश्व में प्रशंसा पा रहे हैं और इनका सहज अनुपालन किया जा रहा है। किंतु हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए यह सब अर्थहीन है।"
आम्बेडकर ने यह उल्लेख किया है कि मनुस्मृति से जर्मन दार्शनिक नीत्शे प्रेरित हुए थे और नीत्शे से प्रेरणा लेने वालों में हिटलर भी था। हिटलर और मुसोलिनी संकीर्ण हिंदुत्व की अवधारणा के प्रतिपादकों के भी आदर्श रहे हैं।
सावरकर भी भारतीय संविधान के कटु आलोचक रहे। उन्होंने लिखा- भारत के नए संविधान के बारे में सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो वेदों के बाद हमारे हिन्दू राष्ट्र के लिए सर्वाधिक पूजनीय है। यह ग्रंथ प्राचीन काल से हमारी संस्कृति और परंपरा तथा आचार विचार का आधार रहा है। आज भी करोड़ों हिंदुओं द्वारा अपने जीवन और व्यवहार में जिन नियमों का पालन किया जाता है वे मनुस्मृति पर ही आधारित हैं। आज मनुस्मृति हिन्दू विधि है।( सावरकर समग्र,खंड 4, प्रभात, दिल्ली, पृष्ठ 416)
गोलवलकर ने बारंबार संविधान से अपनी गहरी असहमति की खुली अभिव्यक्ति की। उन्होंने लिखा- हमारा संविधान पूरे विश्व के विभिन्न संविधानों के विभिन्न आर्टिकल्स की एक बोझिल और बेमेल जमावट है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना कहा जा सके। क्या इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में इस बात का कहीं भी उल्लेख है कि हमारा राष्ट्रीय मिशन क्या है और हमारे जीवन का मूल राग क्या है?(बंच ऑफ थॉट्स, साहित्य सिंधु बेंगलुरु,1996, पृष्ठ 238)
निश्चित ही संविधान में यह नहीं लिखा गया था कि हिन्दू राष्ट्र की स्थापना हमारा राष्ट्रीय मिशन हो और हमारा देश धर्म द्वारा संचालित हो, धर्म ही हमारा मूल राग हो। हमारी संविधान सभा ने तो उस धर्मशास्त्रीय विधिक परंपरा को खारिज कर दिया था जो नारी विरोधी एवं दलित विरोधी थी।दक्षिणपंथियों के आक्रोश का मूल कारण यही था।
जब तक भाजपा के कतिपय वाचाल नेताओं एवं प्रवक्ताओं, कुछ विवादित और विवादप्रिय धर्मगुरुओं तथा झूठ व भ्रम फैलाने वाले आईटी सेल के शरारती तत्वों के माध्यम से संविधान पर आक्रमण किया जा रहा था तब तक यह माना जा सकता था कि यह संविधान के प्रति अनास्था उत्पन्न करने की कोशिशें अवश्य हैं किंतु भारत सरकार इनसे अपनी घोषित एवं अधिकृत सहमति दिखाने का साहस नहीं कर सकती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान की दुर्भावनापूर्ण आलोचना को बौद्धिक गरिमा प्रदान करने की कोशिश की गई है।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा न्याय प्रणाली के भारतीयकरण की मांग उठाई गई है। उच्चतम न्यायालय न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है अपितु यह संविधान का भी संरक्षक है। संविधान के उपबंध की व्याख्या के विषय में अंतिम निर्णय देने का अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त है। यही कारण है कि हमें न्यायपालिका के भारतीयकरण की मांग के निहितार्थों को समझना होगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर ने कहा कि महान वकील और न्यायाधीश पैदा नहीं होते हैं, बल्कि वे मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, नारद, याज्ञवल्क्य एवं प्राचीन भारत के अन्य विधि वेत्ताओं के विचारों के अनुसार तैयार उचित शिक्षा तथा महान विधिक परंपराओं से बनते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्राचीन भारतीय विधिवेत्ताओं के महान ज्ञान की सतत उपेक्षा तथा औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था का निरंतर अनुपालन हमारे संविधान के लक्ष्यों और हमारे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है।
जिस तरह से वर्तमान न्यायप्रणाली पर सवर्णों का वर्चस्व है और जिस प्रकार अभी भी दलितों और आदिवासियों को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है उसके मद्देनजर जस्टिस एस अब्दुल नजीर का कथन चौंकाने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट के अब तक नियुक्त 48 चीफ जस्टिसों में 13 ब्राह्मण रहे हैं। सन 1980 तक सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से कोई भी न्यायाधीश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 256 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है जिसमें से केवल 5 अनुसूचित जाति के और 1 अनुसूचित जनजाति के थे।
सुप्रीम कोर्ट में अब तक नियुक्त महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल 11 है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति 1989 में जाकर हो पाई थी।
1अक्टूबर 2021 की स्थिति में हाई कोर्ट में कार्यरत 627 न्यायाधीशों में केवल 66(10.52 प्रतिशत) महिलाएं थीं। निचली अदालतों की स्थिति और चिंताजनक है।
नेशनल कमीशन फ़ॉर द शेड्यूल्ड कॉस्ट की 2016 की रिपोर्ट यह स्वीकारोक्ति करती है कि जजों की नियुक्ति में अभी भी सवर्ण वर्ग का वर्चस्व है। 2018 में 11 राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार निचली अदालतों में पिछड़े वर्ग के केवल 12 फीसदी,दलित वर्ग के 14 फीसदी जबकि आदिवासी समुदाय के 12 प्रतिशत न्यायाधीश हैं।
अक्टूबर 2021 में द अमेरिकन बार एसोसिएशन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा प्रकाशित चैलेंजेज फ़ॉर दलित्स इन साउथ एशियाज लीगल कम्युनिटी शीर्षक रिपोर्ट में न्यायाधीशों की सवर्ण लॉबी द्वारा दलित न्यायाधीशों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार और दलित न्यायाधीशों की नियुक्ति में बाधा डालने की प्रवृत्ति का विस्तृत जिक्र है।
समय समय पर न्यायाधीशों की सवर्ण मानसिकता जोर मारने लगती है और वे दलित विरोधी निर्णय देने लगते हैं। कुछ नवीनतम उदाहरण दृष्टव्य हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने एससी/एसटी एक्ट 1989 को कमजोर करने वाला एक निर्णय दिया था। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं भी है तब भी सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा कि दलितों और आदिवासियों का आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त एवं प्रभावशाली वर्ग आरक्षण के लाभों को जरूरतमंदों तक पहुंचने नहीं दे रहा है।
नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के 2017 से 2019 के आंकड़े बताते हैं कि दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ हुए अपराधों में अपराध सिद्ध होने की दर केवल 26.86 प्रतिशत रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की मार्च 2021 की एक रिपोर्ट कहती है- अपराध सिद्ध न होने के प्रमुख कारणों में मौजूदा कानूनों का सम्यक क्रियान्वयन न होना तथा इन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी एजेंसियों का असंवेदनशील रवैया भी शामिल हैं। अधिकांश लोगों का बिना दंड पाए निर्दोष सिद्ध हो जाना ताकतवर और प्रभावशाली समुदायों को अत्याचार जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।
दलितों,आदिवासियों एवं महिलाओं के साथ हो रहे शोषण, अत्याचार और भेदभाव के परिप्रेक्ष्य में मनु और अन्य ब्राह्मण वर्चस्व को अनंत काल तक बनाए रखने के इच्छुक विधि वेत्ताओं का अध्ययन केवल एक ही उद्देश्य से किया जा सकता है, वह उद्देश्य है इनके मानवद्रोही चिंतन को बेनकाब करने के लिए ताकि इनके विचार शोषण की किसी भावी रणनीति का आधार न बन सकें।
प्रसंगवश यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हमारे न्यायाधीश अपने फैसलों में मनु और कौटिल्य आदि का उल्लेख करते रहे हैं। जस्टिस एस ए बोबडे ने निजता पर दिए फैसले में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जबकि जोसफ शाइन मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें दूसरे की पत्नी के साथ यौन समागम करने के आदी व्यक्तियों को कठोर दंड देने का प्रावधान है। सबरीमाला मामले में रजस्वला स्त्रियों पर मनुस्मृति में लगाए गए प्रतिबंधों की चर्चा की गई है।
निश्चित ही न्याय प्रणाली का भारतीयकरण एक आकर्षक विचार है, लेकिन भारतीयकरण का अर्थ मनुवादी सोच की पुनर्प्रतिष्ठा और न्याय प्रणाली का ब्राह्मणीकरण तो कतई नहीं है।
इस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार आंबेडकर ने बौद्ध दर्शन परंपरा से लिया है। आदिवासी समाज की लोकतांत्रिक परंपराएं और न्याय प्रणाली चकित करने की सीमा तक मौलिक हैं।
संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था- "मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है- यही वह संबोधन है जो हमें देश के उस हिस्से में दिया जाता है जहां से मैं आता हूँ। एक जंगली - एक आदिवासी के रूप में मुझसे कोई यह उम्मीद नहीं करता कि मैं इस प्रस्ताव की कानूनी बारीकियों को समझ पाऊंगा। किंतु मेरी अपनी सामान्य समझ, मेरे अपने लोगों की सहज बुद्धि मुझे कहती है कि हम सब को स्वतंत्रता और संघर्ष के पथ पर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। महोदय, यदि भारतीय लोगों का कोई ऐसा समूह है जिसके साथ सबसे बुरा बर्ताव किया गया है तो वह मेरे लोग हैं। पिछले छह हजार वर्षों से उनके साथ अपमान और उपेक्षा का व्यवहार किया गया है। यह प्रस्ताव आदिवासियों को प्रजातंत्र नहीं सिखा सकता। आप आदिवासियों को प्रजातंत्र नहीं सिखा सकते, आपको उनसे प्रजातांत्रिक तौर तरीके सीखने होंगे। वे इस दुनिया के सर्वाधिक प्रजातांत्रिक लोग हैं।"
जब हम न्याय प्रणाली के भारतीयकरण की बात करते हैं तब हमें विभिन्न जीवन शैलियों और सांस्कृतिक समूहों की न्याय परंपराओं का आदर करना होगा। आदिवासियों को जबरन हिन्दू धर्म के शोषण मूलक मनुवादी ढांचे को स्वीकारने के लिए बाध्य करने की कोशिशों के नतीजे न पहले अच्छे थे और न अब होंगे।
न्याय प्रणाली के भारतीयकरण को लेकर हो रही चर्चाओं में कानूनी प्रक्रिया पर अंग्रेजी के वर्चस्व को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी प्रावधानों के अनुवाद का सुझाव निश्चित ही स्वागतेय है। किंतु अदालतों एवं पुलिस द्वारा दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले उर्दू-फ़ारसी के बहुत सारे प्रचलित और लोकप्रिय शब्दों से न्याय प्रणाली के भारतीयकरण के हिमायतियों को बैर क्यों है,यह समझ पाना कठिन है। अदालत, मुकद्दमा, गुनाह, गवाह, रोजनामचा, खात्मा, देहाती नालसी, खारिजी, हवाले साना, माल वाजायाफ्ता, मुचलका, जमानत,हवालाती, इश्तहार, तहरीर, गिरफ्तारी, बरी, फरियादी, मुलजिम, मुजरिम, हिरासत, इस्तगासा,मुल्तवी, जिरह, इजरा, तलवी, प्यादा, मुंशी, मुंसिफ, हाजिर, जाहिर सूचना, दरख्वास्त, पतारसी,दीवानी, वकील आदि कितने ही शब्द हैं जिनके प्रयोग के हम अभ्यस्त हैं किंतु इन्हें भी चलन से बाहर करने की कोशिश हो रही है।
यदि न्याय प्रणाली के भारतीयकरण की शुरुआत करनी है तब सरकार को सबसे पहले राजद्रोह कानून(1870),धारा 124 ए, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यूएपीए (1967), सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एएफएसपीए(1958) जैसे औपनिवेशिक मानसिकता के परिचायक कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। किंतु देखने में तो यह आ रहा है कि यह कानून आजकल सरकार को बड़े प्रिय हैं और इनका उपयोग वह असहमत स्वरों को कुचलने के लिए बार बार कर रही है।
न्याय प्रणाली में मनुवादी सोच की पुनर्प्रतिष्ठा के प्रयासों को न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण का नाम दिया जा रहा है। नागरिक अधिकारों और संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय पर यदि ब्राह्मणवादी सोच हावी हो गई तब संविधान पर भी संकट आ सकता है।
रायगढ़, छत्तीसगढ़ स्थित लेखक स्वतंत्र विचारक और टिप्पणीकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।
source ; /hindi.newsclick.in
सोशल मीडिया बोल्ड है। सोशल मीडिया युवा है। सोशल मीडिया सवाल उठाता है। सोशल मीडिया एक जवाब से संतुष्ट नहीं है। सोशल मीडिया बड़ी तस्वीर देखता है। सोशल मीडिया हर विवरण में रुचि रखता है। सोशल मीडिया उत्सुक है। सोशल मीडिया फ्री है। सोशल मीडिया अपूरणीय है। लेकिन कभी अप्रासंगिक नहीं। सोशल मीडिया तुम हो। (समाचार एजेंसी की भाषा से इनपुट के साथ) अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक दोस्त के साथ शेयर करें! हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं। हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक रूप से मदद करें







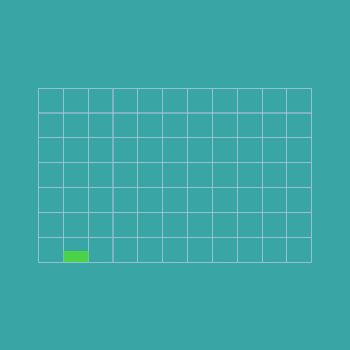







0 Comments