चुनाव आयोग का इलेक्ट्राॅनिक व डिजिटल प्रचार पर निर्भरता को विकल्पहीन बनाना न्यायसंगत नहीं है. दूर-दराज़ के कई क्षेत्रों में अब भी बिजली व इंटरनेट का ठीक से पहुंचना बाकी है, ऐसी जगहों के वंचित तबके के मतदाताओं के पास इतना डेटा कैसे होगा कि वे हर पार्टी के नेता के चुनावी भाषण सुन सके? क्या कोरोना के ख़तरे की आड़ में ऐसे सवालों की अनसुनी की जा सकती है?
पश्चिम बंगाल के एक गांव में एलईडी स्क्रीन पर अमित शाह की वर्चुअल रैली देखते ग्रामीण.
(फाइल फोटो, साभार: ट्विटर)
गत दिनों चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करते हुए रैलियों आदि की मार्फत परंपरागत प्रचार पर रोक लगा दी, जिससे पार्टियों व प्रत्याशियों को अपने विचारों व नीतियों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल आदि विभिन्न मीडियारूपों का ही सहारा रह गया, तो बहुत से लोगों को मई, 1982 की याद आई.
तब चुनाव आयोग ने केरल के एर्नाकुलम जिले के परवूर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में 84 में से पचास बूथों पर मनमाने तौर पर मतदान की प्रक्रिया बदलकर उसमें बैलेट पेपरों के बजाय इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर लिया था.
तब तक 1551 के जनप्रतिनिधित्व कानून और 1961 के चुनाव कानून में ऐसे किसी बदलाव की व्यवस्था नहीं थी. शायद इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बदलाव को ट्रायल बताया था. लेकिन इसके बाद का उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा.
उक्त चुनाव में हुए बेहद नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी एसी जोस, जो राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, मामूली वोटों के अंतर से हार गए तो हाईकोर्ट चले गए, जहां उन्होंने अपनी याचिका में सवाल उठाया कि क्या संसद द्वारा जनप्रतिनिधित्व व चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का प्रावधान किए बगैर चुनाव आयोग को अपनी ओर से बैलेट पेपर के बजाय मशीनों से मतदान कराने का अधिकार है?
हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी तो भी उन्होंने हार नहीं मानी. अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली और फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग को विधिसम्मत प्रक्रिया से चुनाव कराने का ही अधिकार है, उसे बदलने का नहीं. न्यायालय ने उन 50 बूथों पर, जहां आयोग ने मशीनों से मतदान कराया था, फिर से बैलेट पेपर से मतदान कराने का आदेश दिया, जिसका अनुपालन हुआ तो जोस को 2,000 वोट ज्यादा मिले.
न्यायालय के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग को इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल रोक देना पड़ा. बाद में संसद ने संबंधित कानून में संशोधन करके उनके उपयोग का रास्ता साफ किया तो उन्हें फिर से इस्तेमाल किया जाने लगा. हाल में इन मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे तो चुनाव आयोग ने वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों का प्रयोग भी शुरू किया.
अब यह कानून के जानकारों के विश्लेषण का विषय है कि पार्टियों व प्रत्याशियों को परंपरागत चुनाव प्रचार से वंचित कर इलेक्ट्राॅनिक या डिजिटल माध्यमों पर निर्भर बनाना उस अर्थ में चुनाव प्रक्रिया को बदलना है या नहीं, जिस अर्थ में सुप्रीम कोर्ट ने बिना संसद की अनुमति के चुनाव आयोग द्वारा बैलेट पेपरों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को इस प्रक्रिया का बदलना ठहराया था.
लेकिन जिस तरह कई छोटे दल और निर्दल प्रत्याशी इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल प्रचार में खुद को असहज व कमजोर महसूस कर रहे, जबकि साधन व धन संपन्न दल व प्रत्याशी गदगद हैं, उससे यह अंपायर द्वारा मुकाबले में सभी प्रतिद्वंद्वियों को समान अवसर देने व सबके साथ समान व्यवहार करने के सिद्धांत का चुनावों की स्वतंत्रता व निष्पक्षता पर असर डालने वाला गंभीर उल्लंघन लगता है.
अकारण नहीं कि जब से चुनाव आयोग ने यह फैसलाकर मतदाताओं तक पहुंचने के लिए दलों व प्रत्याशियों के समक्ष मीडिया और वर्चुअल रैली के माध्यम से डिजिटल प्रचार के ही विकल्प छोड़े हैं, तभी से सवाल उठाए जाने लगे हैं कि क्या उसके इस फैसले का मुकाबले के सभी पक्षों पर एक जैसा असर होगा? अगर नहीं तो इसका लाभ किसके खाते में जाएगा?
जानकारों के अनुसार केंद्र व उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनावी चंदा हासिल करने में तो अपने प्रतिद्वंद्वी दलों से आगे और सबसे अमीर है ही, इलेक्ट्राॅनिक व डिजिटल प्लेटफार्मों पर भी बढ़त हासिल किए हुए है.
समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव शायद इसी के मद्देनजर कहते हैं, ‘हम झंडा, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग कुछ लगा नहीं सकते. जनसभाएं व रोड शो कर नहीं सकते. मीडिया है कि विपक्ष को दिखा नहीं सकता. तो क्या चुनाव आयोग द्वारा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ती भीड़ से घबराई सरकारी पार्टी के अनकूल व्यवस्था की जा रही है?’
दूसरी ओर जानकार भी पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस तथ्य की जानकारी नहीं है या उसने सोची-समझी रणनीति के तहत भाजपा के लिए बढ़त पाने का रास्ता तैयार किया है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कब्जा जमाए बैठे उसके लोग, साथ ही ट्रोल आर्मी, उसके काम आ सके.
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है कि जिन पार्टियों के पास संसाधन नहीं है, वे वर्चुअल रैली कैसे करेंगी और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रचार की दौड़ में उन्हें स्पेस कैसे मिलेगा? क्या इसके लिए चुनाव आयोग उन्हें धन और संसाधन उपलब्ध कराएगा?
उनका सवाल इस अर्थ में भी प्रासंगिक है कि ट्विटर, फेसबुक व वॉट्सऐप जैसे तमाम सोशल मीडिया ऐप भी भाजपा की कहें या उसकी सत्ता की मुट्ठी में ही हैं. लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की मानें तो बात इतनी-सी ही नहीं है और व चुनावों की जीत-हार तक ही सीमित है.
उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट में लिखा कि बुली बाई ऐप मामले में अभियुक्तों की कम उम्र देखकर पूरा देश पूछ रहा था कि इतनी नफरत आती कहां से है? दरअसल भाजपा ने नफरत की कई डिजिटल फैक्ट्रियां लगा रखी हैं.
राहत की बात यह है कि अब भाजपा के अपने भी इसके खिलाफ मुखर हो रहे हैं. उसकी आईटी सेल की एक पूर्व महिला महिला कार्यकर्ता का कहना है कि उसके द्वारा टेक फॉग नाम के ऐप का इस्तेमाल अपने आलोचकों को प्रताड़ित करने और जन धारणाओं को अपनी ओर मोड़ने के लिए किया जाता है.
कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को लेकर भी भाजपा पर ऐसे आरोप लग चुके हैं. यह भी खबर है कि उसने डिजिटल प्रचार के लिए 8,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रखा है और उसके पास अपनी विशाल आईटी आर्मी का खर्च उठाने के लिए भरपूर संसाधन भी हैं.
साफ है कि चुनाव आयोग का इलेक्ट्राॅनिक व डिजिटल प्रचार पर निर्भरता को विकल्पहीन बनाना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है. ठीक है कि युवा नेताओं और मतदाताओं को प्रचार के डिजिटल माध्यमों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनेक उम्रदराज नेता व मतदाता अभी भी उनसे अछूते है. या उन्हें लेकर असहज महसूस करते हैं.
दूर-दराज के कई क्षेत्रों में अभी भी बिजली व इंटरनेट का ठीक से पहुंचना बाकी है, जो इन माध्यमों के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है. डिजिटल इंडिया में अभी शाइनिंग इंडिया और फील गुड वाले लोग ही ज्यादा हैं.
ऐसे में इलेक्ट्राॅनिक या डिजिटल प्रचार पर ही निर्भर पार्टियां वृद्ध मतदाताओं तक अपनी बात किस तरह पहुंचा पाएंगी? पहुंचाएंगी भी तो उसमें उनके समवयस्क नेताओं की आवाजें कैसे शामिल करेंगी? नहीं शामिल कर पाएंगी तो क्या इन चुनावों में युवा नेता और युवा मतदाता ही जीत और हार तय करेंगे?
दूर-दराज के गांवों और शहरों के दलित व वंचित तबके के मतदाताओं के पास इतना डेटा क्योंकर होगा कि वे हर पार्टी के नेताओं के चुनावी भाषण सुन सके? क्या कोरोना के खतरे की आड़ में इन सारे सवालों की अनसुनी की जा सकती है?
खतरा है तो क्या यह बेहतर नहीं होता कि सारा तकिया इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रचार पर रखने से पहले चुनाव आयोग खुद को इस सवाल के सामने कर लेता कि इससे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर कितना गंभीर असर पड़ेगा?
इस असर को टालने के लिए परंपरागत प्रचार से महरूम किए गए सारे दलों व प्रत्याशियों को प्रचार के नए साझा डिजिटल मंच क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा सकते, जिससे उनकी इस संबंधी सहूलियतों में समरूपता रहे?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)
सोशल मीडिया बोल्ड है। सोशल मीडिया युवा है। सोशल मीडिया सवाल उठाता है। सोशल मीडिया एक जवाब से संतुष्ट नहीं है। सोशल मीडिया बड़ी तस्वीर देखता है। सोशल मीडिया हर विवरण में रुचि रखता है। सोशल मीडिया उत्सुक है। सोशल मीडिया फ्री है। सोशल मीडिया अपूरणीय है। लेकिन कभी अप्रासंगिक नहीं। सोशल मीडिया तुम हो। (समाचार एजेंसी की भाषा से इनपुट के साथ) अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक दोस्त के साथ शेयर करें! हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं। हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक रूप से मदद करें !






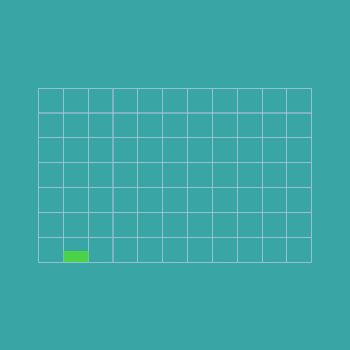






0 Comments